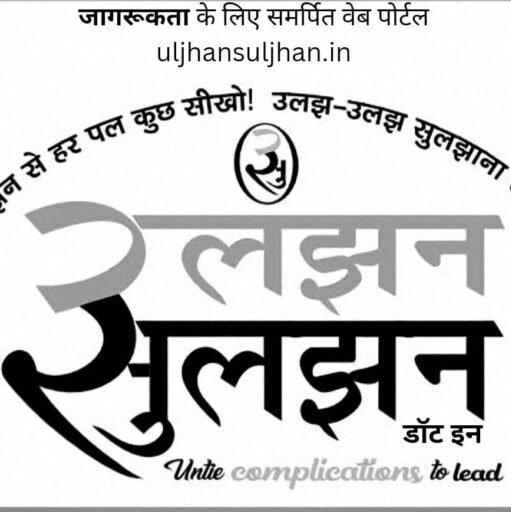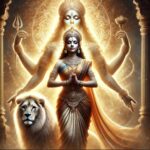मनुष्य के लिए जीवन और मृत्यु सदा से जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इस भौतिक संसार से परे, मृत्यु के पश्चात परालौकिक संसार के रहस्यों को जानने की उत्सुकता हर युग में बनी रही है। विभिन्न संस्कृतियों में, समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार, मृत्यु के पश्चात की स्थिति की भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की गई हैं। ये कल्पनाएँ धर्म, मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं के साथ निरंतर परिवर्तित होती रही हैं। जो धर्म और संस्कृतियाँ पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, वे जीवन के अंत को ही अंतिम सत्य मानते हैं।
वहीं, कुछ संस्कृतियों में यह धारणा रही है कि मृत्यु के बाद भी एक यात्रा जारी रहती है। समय-समय पर इसके प्रमाण भी मिले हैं, जैसे—मिस्र की महान सभ्यता में कब्रों (ममियों) के साथ उपयोगी वस्तुओं का पाया जाना, या सिंधु घाटी सभ्यता में मानव कंकालों के साथ आभूषण, चूड़ियाँ और पालतू जानवरों के अवशेषों की उपस्थिति। ये संकेत करते हैं कि मृत्यु के बाद भी किसी अस्तित्व की संभावना पर विश्वास किया जाता रहा है।
मनुष्य जैसे-जैसे सभ्यता की यात्रा में आगे बढ़ा, उसने अपने रीति-रिवाजों के अनुसार मृत्यु उपरांत किए जाने वाले संस्कारों को विकसित किया। इन्हीं में से एक है मृत्यु भोज।
मृत्यु भोज:परंपरा का स्वरूप और बदलाव
अधिकांश संस्कृतियों में मृत्यु को शोक का प्रतीक माना गया है। परंतु संभवतः प्राचीन काल में, जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों को पूर्ण कर दीर्घायु प्राप्त करता था, तब उसकी स्मृति में एक सामूहिक भोज आयोजित करने की परंपरा प्रारंभ हुई होगी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं—जैसे उस समय यातायात के अभाव में दूर-दूर से आए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था, गरीबों को भोजन कराकर धार्मिक लाभ की कामना, अथवा पशु-पक्षियों को अन्नदान करने की भावना।
परंतु धीरे-धीरे यह परंपरा अपने मूल उद्देश्य से भटक गई और एक अनिवार्य सामाजिक अनुष्ठान का रूप ले बैठी। प्रारंभ में मृत्यु भोज व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार आयोजित होता था, लेकिन कालांतर में यह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। आज यह प्रथा एक विनाशकारी कुरीति में परिवर्तित हो चुकी है।
क्या मृत्यु भोज आवश्यक है?
जहाँ मृत्यु के अवसर पर परिवार शोकाकुल होता है, करुण क्रंदन गूँजते हैं और वे अपने प्रियजन को खोने के दुःख में डूबे होते हैं, वहाँ उत्सव की भाँति भव्य भोज आयोजित करना क्या उचित है? क्या उस कठिन समय में, जब परिवार को मानसिक सहारे की आवश्यकता होती है, छप्पन भोग प्रसंगिक है?
मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि के लिए वर्षों तक धन संचय करता है। आजकल लोग स्वास्थ्य बीमा लेकर बीमारियों से बचाव के प्रयास कर रहे हैं। जन्म की पूर्व सूचना कई माह पहले मिल जाती है, लेकिन मृत्यु अप्रत्याशित होती है—ऐसे असीम दुःख के क्षण में व्यक्ति को मानसिक संबल चाहिए या इस कुरीति रूपी उत्सव को निभाने की बाध्यता?
दुर्भाग्य से समाज में झूठी प्रतिष्ठा दिखाने की होड़ में “कर्ज लेकर भी घी पीने” की प्रवृत्ति न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर चुकी है और करती जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में यह कुरीति इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि कई स्थानों पर मृत्यु भोज में शराब तक परोसी जाती है। परिवार कर्ज के जाल में फँस जाते हैं, घर-जमीन तक बिक जाती है। जो धन शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, वह इस आडंबर में नष्ट हो रहा है।
यदि कोई इस परंपरा का विरोध करने की हिम्मत करता है या आर्थिक असमर्थता के कारण इसे नहीं निभा पाता, तो उसे सामाजिक तिरस्कार सहना पड़ता है। ग्वालियर संभाग में प्रवास के दौरान एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वर्ष 2010 के आसपास उन्होंने मृत्यु भोज में लगभग 10 से 12 लाख रुपये खर्च किए—जो एक शादी के खर्च के बराबर था। कल्पना कीजिए, यदि यह धन बच्चों की शिक्षा में लगाया जाता, तो उस परिवार की स्थिति कितनी सकारात्मक हो सकती थी!
साक्षर लोग भी बढ़ावा क्यों दे रहे हैं?
सबसे दुखद पहलू यह है कि शिक्षित वर्ग भी इसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बढ़ावा दे रहा है। लोग इसे एक अनिवार्य संस्कार मान चुके हैं, जबकि यह केवल एक अनावश्यक खर्च और सामाजिक बोझ है। सक्षम लोग इसे भव्य रूप देकर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की स्थिति और कठिन बना रहे हैं।
यद्यपि, कई स्थानों पर जागरूकता आई है और इस कुरीति में कमी भी देखी गई है। कुछ समाजों में इसे पूरी तरह निषिद्ध कर दिया गया है। ग्वालियर संभाग में संत श्री गिरी हरि महाराज जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से यह कुरीति काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संभाग में भी कुछ समुदायों ने इसे पूरी तरह त्याग दिया है।
क्या हमें आत्ममंथन की आवश्यकता नहीं?
हमें स्वयं आत्मचिंतन करना होगा कि—
- क्या मृत्यु भोज सच में अनिवार्य है?
- क्या शोक के समय स्वादिष्ट व्यंजनों का आयोजन उचित है?
- क्या केवल प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कर्ज लेकर यह अनावश्यक खर्च करना सही है?
समाज के बुद्धिजीवियों, युवाओं, शिक्षाविदों और वरिष्ठ नागरिकों को संगठित होकर इस कुरीति के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करना चाहिए। जब तक हम सामूहिक रूप से इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक यह समाप्त नहीं होगी।
हमें आशा है कि यह सवेरा जल्द आएगा!
रचयिता
श्री समीर पंवार
सहारनपुर
प्रस्तुति