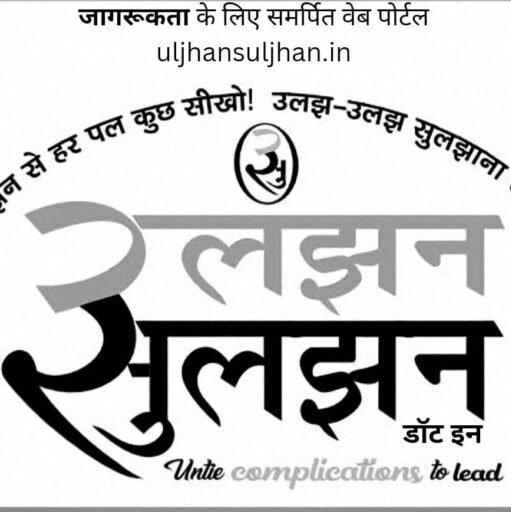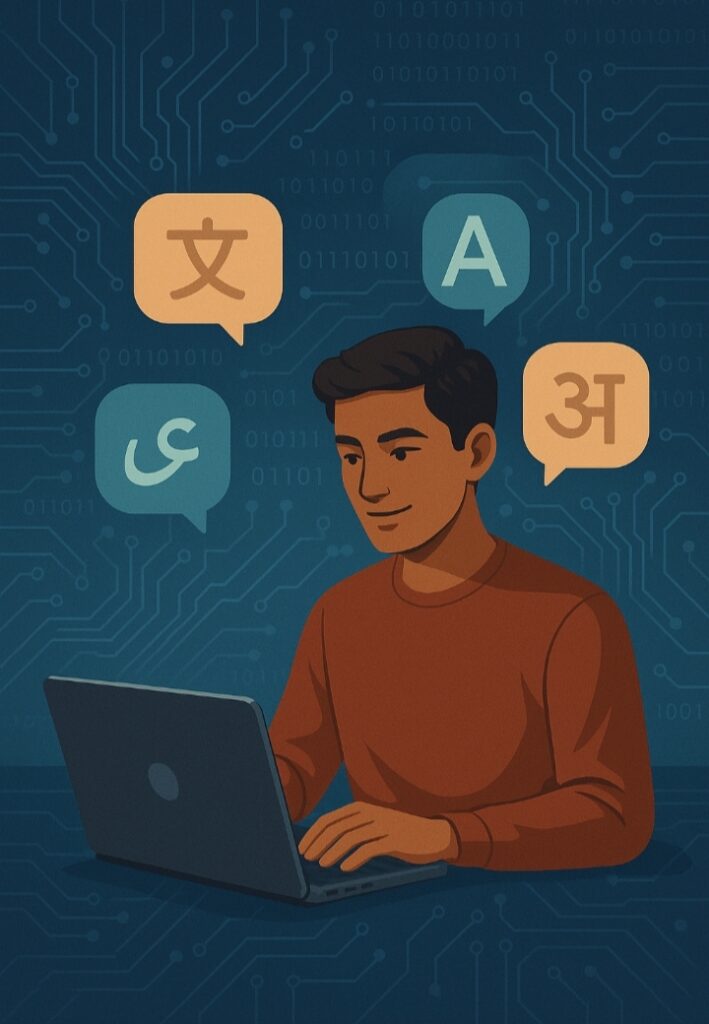तकनीकी सफलता के युग में भाषाओं की स्थिति
भाषा मूलतः किसी भी समाज की आत्मा होती है। यह न केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की संवाहिका भी है। प्रत्येक भाषा ने समय के साथ विद्वानों की सहायता से अपने लिए एक ठोस ढांचा विकसित किया — जिसमें शब्दकोश, व्याकरण, लिपि और उच्चारण के साथ साथ उसकी मर्यादाएं भी शामिल हैं। इन मर्यादाओं का उद्देश्य था — हमारी अभिव्यक्ति को स्पष्ट, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाना।
व्याकरण – भाषा की रीढ़
किसी शरीर को साधने के लिए जिस प्रकार रीढ़ की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी भाषा को साधने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए व्याकरण की अनिवार्यता है जो भाषा की संरचना को स्थिर और संतुलित बनाती है। एक-एक शब्द, एक-एक क्रिया और उनका सही क्रम भाषा को धार देता है। संस्कृत, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, बंगाली — हर भाषा में भाषाई सुधारवादियों ने शब्दों और उनके उपयोग को लेकर निरंतर गहन शोध किया, परिश्रम किया, और उन्हें व्याकरणिक ढांचे में बांधा। यह केवल नियमों की बात नहीं थी, यह श्रद्धा थी, अपने संवाद को सटीक और अधिकाधिक उपयोगी बनाने की एक साधना थी।
आज का यथार्थ: तकनीकी प्रगति में भाषाई गिरावट
आज हम तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया और त्वरित संचार के साधनों ने संवाद को सरल बना दिया है — पर यक्ष प्रश्न यह है कि
क्या यह संवाद पूर्ण और परिपक्व भी है?
आज हम संक्षिप्तीकरण, अपभ्रंश और मिश्रित भाषा (हिंग्लिश, टिंग्लिश आदि) के ऐसे दौर में हैं जहाँ न शब्दों का सही रूप बच पा रहा है, न व्याकरण का पालन।

भाषा की स्वतंत्रता या स्वेच्छाचारिता?
आज यह तर्क दिया जाता है कि भाषा को स्वतंत्र होना चाहिए — जैसा मन करे, वैसे बोले या लिखें। पर वास्तव में क्या यह स्वतंत्रता है या लापरवाही? जब हम ‘हूँ’, ‘था’, ‘है’, ‘रहा’ जैसी साधारण सहायक क्रियाओं का प्रयोग तो गलत करते ही हैं, जब हम ‘आप’ के साथ ‘करता हूँ’ जोड़ते हैं, जब हम लिंग, वचन, काल, कारक जैसे मूल नियमों की अनदेखी करते हैं — तो हम अभिव्यक्ति को नष्ट कर रहे होते हैं। बात केवल गलती की नहीं है, बात उस भाव की हत्या की है जो किसी वाक्य में छुपा था और जो व्याकरणिक असावधानी से खो गया।
भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है — वह सोचने का आधार है।
जब हम भाषा को हल्के में लेने लगते हैं, तो हम सोचने की प्रक्रिया को भी कमजोर करते हैं। आज सोशल मीडिया पर कई विचार अधूरे, असंतुलित और अस्पष्ट रहते हैं — कारण है भाषा की वह अव्यवस्था, जिसने विचार की गहराई को सतही बना दिया है। अति उत्साह में सोशल मीडिया का आकर्षण सभी को आकर्षित तो करता है लेकिन वृहद शब्द ज्ञान उसकी अनिवार्यता है यह हम ध्यान में नहीं रख पाते।
समाधान क्या है?
हमें भाषा से फिर से प्रेम करना होगा। जैसे एक कलाकार अपने ब्रश और रंगों से प्रेम करता है, वैसे ही हमें शब्दों और व्याकरण से लगाव पैदा करना होगा। हमें बच्चों को न केवल नई भाषा सिखानी चाहिए, बल्कि उनकी अपनी मातृभाषा का सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। हमें यह याद दिलाना होगा कि भाषा केवल संप्रेषण नहीं, संवेदनाओं का वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है।
अंत में
तकनीक ने संवाद को तेज़ किया है, पर भाषा ही है जो उसे अर्थ देती है। अगर हमने भाषा को ही खो दिया, तो हम केवल शोर करेंगे — संवाद नहीं। आइए, इस आधुनिक युग में, भाषाओं की गरिमा को बचाए रखें — व्याकरण, उच्चारण, और शब्दों की आत्मा को समझते हुए। यह केवल भाषा का नहीं, हमारी सोच, संस्कृति और आत्मा का प्रश्न है।
आइडिया
शब्दशिल्प
पाठ्य विस्तार
चैट जीपीटी
प्रस्तुति