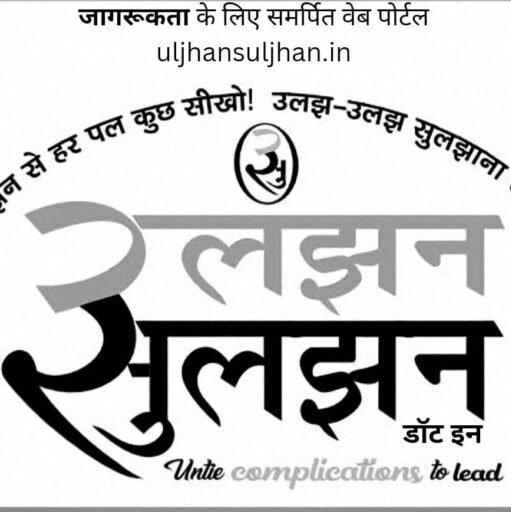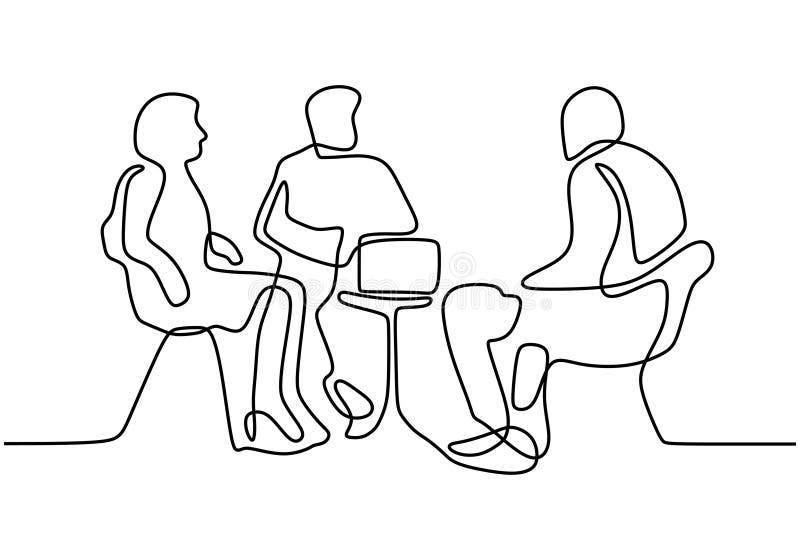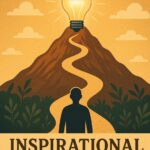गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल आवश्यक क्यों?
प्रोफेसर (डॉ.) राकेश राणा
यह एक प्राकृतिक और मौलिक व्यवस्था है कि
किसी भी इकोसिस्टम का उपभोक्ता ही गुणवत्ता का अनुभव कर पाता है। इसी तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था में छात्र, अभिभावक, प्रबंधन-तंत्र और अंततः समग्र समाज अपने-अपने दृष्टिकोण से शिक्षा की गुणवत्ता का गुणगान करते हैं। भारत जैसे वैविध्यपूर्ण समाज में गुणवत्ता के पैमाने तय कर पाना और भी मुश्किल है। हमारे समाज की विविधताएँ, विभिन्नताएँ, स्थानीय आवश्यकताएँ और प्राथमिकताएँ बहुत विचित्र हैं। इन विरोधाभासों में संतुलन साधने के लिए शिक्षा व्यवस्था को अतिरिक्त भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सवाल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण, संसाधन और मूल्यांकन सहित शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलू समाहित हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु कुशलता के साथ शिक्षण उपकरणों का उपयोग करते हुए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और आर्थिक-सामाजिक स्थिति एवं स्थान की परवाह किए बिना एक सहायक शैक्षिक वातावरण बनाने का एल्गोरिदम है।
वास्तव में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समग्र विकास का अजस्र स्रोत है। शिक्षा बच्चे के व्यक्तिगत विकास के माध्यम से उसमें आत्मविश्वास और आत्म-मूल्यों का रोपण करती है। सामाजिक और आर्थिक उन्नति में छात्र को उत्पादक बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने योग्य बनाती है। उसे जीवन के लिए तैयार करती है, चुनौतियों से निपटना सिखाती है। शिक्षा विश्व के वास्तविक चतुर्मुखी विकास की धुरी है। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। यहाँ पर प्रश्न सामाजिक महत्व का भी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आवश्यक आधार कैसे तैयार हो और इस महान भूमिका के लिए कौन आगे आए। इस बहस के ढेरों आयाम हैं। शिक्षा को वास्तव में उच्च-गुणवत्तापूर्ण बनाता क्या है? नि:संदेह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कई प्रमुख तत्व हैं जो एक साथ मिलकर एक मजबूत और प्रभावी शैक्षिक परिवेश का निर्माण करते हुए शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन मुख्य घटकों में स्कूल, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय प्रबंधन-तंत्र, प्रशासन, अधोसंरचना, संसाधन, तकनीकी और समुदाय सब कुछ समाहित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये तमाम घटक जहाँ संयुक्त अभ्यास करते हैं, वह है विद्यालय–स्कूल। अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल का अच्छा होना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक अच्छा स्कूल समावेशी शैक्षिक संस्कृति के निर्माण पर ध्यान देता है।
एक गुणवत्तापूर्ण संस्थान में शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और प्रबंधन-तंत्र तक का रवैया बहुत सकारात्मक और खुशमिजाजी वाला होगा; वहाँ सबकी सब तक पहुँच सहज और सुलभ होगी।
ऐसे स्कूल का दृष्टिकोण पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षण सामग्री के डिज़ाइन और डिलीवरी तक विद्यार्थी-केंद्रित होगा।
ऐसे स्कूल के शिक्षक सामान्यतः खुश और संतुष्ट नज़र आएँगे। संस्थान नियमित रूप से अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देगा।
ऐसे स्कूल में एक सशक्त छात्र गतिविधि विभाग सक्रिय होगा, जिसमें खेल से लेकर साहित्यिक, मनोरंजनात्मक और संवाद व सहयोग के स्रोत सक्रिय दिखेंगे।
गुणवत्तापूर्ण स्कूल की अंतिम पहचान यही होती है कि वह अपनी पहचान का प्रचार कैसे करता है? अपनी पहचान किन चीजों के ज़रिए समाज में पहुँचाना चाहता है। बच्चों के ऊँचे स्कोर के इर्द-गिर्द अपने संदेश को केंद्रित करता है या अपनी एक अभिजात्य छवि बनाने की दिशा में कोई और विशिष्टता अपनाता है। इन सब छद्म छवियों से आगे बढ़कर एक अच्छा स्कूल उन बातों पर ज़ोर देता है, अपनी उन चीजों का प्रचार-प्रसार करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह ध्यान रहे, एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण स्कूल का संदेश छात्रों की सहभागिता और अभिभावकों की संतुष्टि पर केंद्रित होगा। अच्छे स्कूल प्रदर्शन में आस्था नहीं रखते; वे अपना एक अलग दर्शन विकसित करते हैं।
हमेशा एक अच्छे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था लचीली और सस्ती होती है। अच्छा स्कूल नई तकनीकों और विधियों के विस्तार में आस्था रखता है। जैसे संचार क्रांति का उपयोग कोई स्कूल अपनी छद्म विशिष्टता बनाए रखने में भी कर सकता है और समाज में शिक्षा के विस्तार की दिशा में उपयोग करते हुए शिक्षा को भौगोलिक रूप से स्वतंत्र भी कर सकता है तथा अधिकतम लोगों तक ज्ञान की पहुँच सुलभ बना सकता है।
अच्छे स्कूल की संस्कृति समावेशी होती है; वहाँ बच्चों से लेकर शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, प्रबंधन-तंत्र तथा बाह्य सहायकों तक में वैविध्य दिखेगा।
एक अच्छे स्कूल की पहचान यह भी है कि वह अपने बच्चों को निरंतर स्कूलेत्तर अनुभवों से जोड़ने के नए-नए तरीकों को खोजने की दिशा में संलग्न हो।
अच्छे स्कूल के लिए सर्वाधिक महत्व इस बात का भी है कि स्कूल कितना सुरक्षित है, वह आधुनिक संसाधनों से कितना सुसज्जित है और अंततः वह सामाजिक रूप से कितना सरोकार रखता है।
एक अच्छे स्कूल के लिए शिक्षा का गंतव्य परीक्षा नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा होती है। ऐसे स्कूल में विद्यार्थी एक व्यापक जीवन दृष्टिकोण का अभ्यास करते हैं।
एक अच्छे स्कूल के योग्य शिक्षक नई-नई शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं।
एक अच्छा स्कूल नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धति का प्रयोग करता है, परिणामतः बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, सामूहिकता और समस्या समाधान सीखाता है, टीम स्पिरिट सिखाता है।
अच्छा स्कूल सक्रिय मूल्यांकन करता है। वह अंकों से आगे जाकर सतत मूल्यांकन की संस्कृति विकसित करता है और फीडबैक के नए-नए तौर-तरीके खोजता है।
अच्छे स्कूल में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया जाता है। अच्छा स्कूल इस सामाजिक दायित्व का बोध भी रखता है कि बच्चा स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक भलाई भी सीखे।
**निष्कर्षतः** अच्छा स्कूल पढ़ाई के पार जाकर सोचता और समझता है। ऐसा स्कूल कुल मिलाकर शैक्षिक घटकों के साथ समन्वय स्थापित करता है और उत्तरोत्तर सुधार की दिशा में सोचता है। एक अच्छा विद्यालय ही समाज के भविष्य को भाँप सकता है। हर नई पीढ़ी को गढ़ता है और हर कदम विकास की अगली सीढ़ी चढ़ता है। यह उद्यम विद्यालयों में ही संभव है, जहाँ समाज के परिष्कार के लिए सतत संधान चलता है। इसलिए एक स्कूल अथक परिश्रम में संलग्न रहते हुए नवाचारों को नवोन्मेषी दृष्टि से लेता है और नवप्रवर्तनों का स्वागत करता है। मौजूदा समय में तकनीक जिस तरह शैक्षिक परिदृश्य को बदल रही है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के तौर-तरीके और उन्हें शिक्षा देने की तकनीकें बदल गई हैं। ऐसे में नया स्कूल कुछ अतिरिक्त भूमिकाओं में सामने आएगा। अब हम एक बदलती वैश्विक दुनिया का हिस्सा हैं। 21वीं सदी की पहली चौथाई को जी लेने के बाद यह सवाल और भी मौजूं हो जाता है कि भविष्य का स्कूल कैसा होगा।
भविष्य का स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देने वाला तो होगा ही, साथ ही सबको शिक्षा भी मुहैया कराना उसका नैतिक दायित्व होगा।
भविष्य के स्कूल अनुकूल शिक्षण पद्धतियों पर ज़ोर देंगे और अपने छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझेंगे, क्योंकि भावी पीढ़ी भावनात्मक स्वास्थ्य के संकट का सामना करेगी।
भावी शैक्षिक परिदृश्य बहु-विषयों के पाठ्यक्रम की मांग करेगा। हर बच्चा सब कुछ सीखे और अपडेटेड शिक्षा सामग्री तक पहुँच रखे। स्कूल को अपने शिक्षण संसाधनों को ऐसे संयोजित करना होगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि सब पढ़े, सब आगे बढ़े।
भविष्य का स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आर्थिक और वित्तीय स्वतंत्रताओं के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता पर रखेगा। तभी वह अपनी वास्तविक सामाजिक-अकादमिक भूमिका का ईमानदार निर्वहन कर रहा होगा।
भविष्य के स्कूल को देर-सबेर यह भी समझना होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो सबसे मिसिंग पार्ट है, वह है भावनात्मक पक्ष, जिस पर बात करने से अक्सर बचा जाता है। स्कूल और शिक्षक ने माताओं के हिस्से का एक बड़ा समय बच्चों के साथ बिताए जाने वाला छीन लिया है। तब क्यों न उन्हें एक सहायक अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा? क्योंकि परिवार (माता-पिता) की इस भूमिका से वंचित हो जाने के परिणामस्वरूप बच्चे भावनात्मक रूप से पिछड़ रहे हैं।
विश्व समाज को कमजोर करने वाले, हमारे आपसी संबंधों को क्षीण करने वाले अंधाधुंध उपभोक्तावाद ने, बढ़ते पर्यावरणीय संकट ने, वैश्विक आतंक-हिंसा ने और बढ़ती गैर-बराबरी ने जिस तरह से मानवीयता को खरोंचा है, ऐसे में एकमात्र आशा शिक्षा ही बचती है जहाँ से समाज सुधार की संभावनाएँ जग सकती हैं। स्कूल ही इस आह्वान को कर सकते हैं, जो व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण तक पहुँच सकता है। इसकी शुरुआत स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, उसके दार्शनिक पक्ष से करनी होगी। वह शिक्षा ही क्या जो व्यक्ति को दार्शनिक दृष्टिकोण न दे। वह दार्शनिकता ही है जो व्यक्ति को संवेदनशील, सहयोगी और सामाजिक रूप से सरोकार रखने वाला बनाती है।
इन पुनीत दायित्वों का निर्वहन कोई शिक्षण संस्थान सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देकर ही कर सकता है। ऐसे स्कूल ही छात्रों को दार्शनिक रूप से उदार बनने में मददगार हो सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से प्रभावशाली, क्षमाशील और कुछ हद तक संतुष्ट बनाता है। कोई स्कूल अपने दृष्टिकोण का विकास अपने इन्हीं अभ्यासों के ज़रिए करता है। अच्छा स्कूल अपनी सर्वोत्तम परंपराओं और संबंधों का मॉडल अपनी उस आदर्श छवि में निर्मित करता है, जिसमें समाज को विश्वास और प्रयास साक्षात दिखता है। अच्छे स्कूल की हर गतिविधि का केंद्र विद्यार्थी होता है। वह हर स्तर पर जवाबदेही और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को समानांतर रखता है। अच्छे स्कूल का कण-कण कहता है—“मैं बच्चे को बेहतर ढंग से सीखने में कैसे मददगार बन सकता हूँ।”