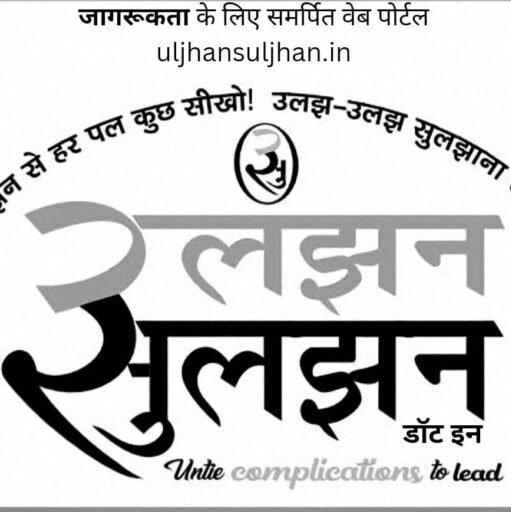दहेज : समाज का बहुरंगी लेकिन काला सच
भारतीय समाज की विविध बिरादरियों में दहेज प्रथा आज भी ऐसी ही मजबूती से जकड़ी हुई है जैसे किसी अतीत की बेड़ी। शिक्षा, आधुनिकता और आर्थिक प्रगति के दावों के बावजूद, यह कुप्रथा जाति और वर्ग विशेष के अनुसार अलग-अलग स्वरूपों में जीवित है।
आई.ए.एस. या उच्च पदों का ‘रेट’
आज स्थिति यह है कि दहेज एक प्रकार का खुला बाज़ार बन चुका है। आई.ए.एस. और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित दूल्हों का “रेट” करोड़ों में पहुँच गया है। विवाह एक सामाजिक और मानवीय संबंध से अधिक, एक सौदे की तरह देखा जाता है। यह विडंबना है कि मिज़ोरम जैसे किसी कम महत्व वाले राज्य का कैडर मिलने पर उस अधिकारी की कीमत घट जाती है—यानी योग्य व्यक्ति की पहचान उसकी सेवाभावना या कर्मठता से नहीं, बल्कि उसके कैडर और संभावित कमाई से होती है।
अन्य सेवाओं की स्थिति
* सिपाही बनाम शिक्षक : समाज में यह धारणा भी गहरी है कि पुलिस सेवा में ऊपरी कमाई के अवसर ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ दहेज की मांग शिक्षक से कहीं अधिक है।
* डॉक्टर : समाज के सबसे सेवा भावी वर्ग—डॉक्टर—को भी सम्मानजनक स्थान तो मिलता है, परंतु उनके विवाह में स्वागत और आदर का स्वरूप किसी महासभा में देखने को नहीं मिलता। उनकी सेवाएँ जीवन-मरण से जुड़ी हैं, फिर भी उन्हें दहेज की दौड़ में वही स्थान नहीं मिल पाता जो आई.ए.एस. या प्रशासनिक पदों को मिलता है।
* समाजसेवी : समाज सुधार के लिए निस्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का तो कभी किसी बिरादरी ने सामूहिक अभिनंदन तक नहीं किया। वे बिना किसी भत्ते या पद के, अपने संसाधनों से समाज की भलाई में जुटे रहते हैं, फिर भी विवाह बाज़ार में उनका कोई मूल्यांकन नहीं होता।
दहेज की परिभाषा
दहेज वास्तव में क्या है?
लेखक के शब्दों में—
“नाकाबिल औलाद को काबिल औलाद के गले में रुपया के बल पर घालने को दहेज कहते हैं।”
यह परिभाषा सटीक और व्यंग्यात्मक दोनों है। विवाह, जो दो आत्माओं और परिवारों का पवित्र बंधन होना चाहिए, धन की ताकत से मजबूरी का बंधन बन जाता है।
एक ताज़ा उदाहरण
किसी आई.ए.एस. अधिकारी के विवाह के लिए एक परिचित ने पाँच करोड़ का प्रस्ताव रखा। दूल्हे के पिता ने दस करोड़ की मांग की और सौदा सात करोड़ तक पहुँचा, परंतु बात नहीं बनी। यह केवल एक उदाहरण है, पर यह दिखाता है कि कैसे समाज के सम्पन्न वर्ग किसी अधिकारी को पाने के लिए बोली लगाने को तैयार रहते हैं।
विविध जातीय परिप्रेक्ष्य
प्रत्येक बिरादरी में दहेज का स्वरूप भिन्न है।
* समृद्ध और उच्चवर्गीय जातियाँ अधिकतर धन और पद को प्राथमिकता देती हैं।
* मध्यम वर्गीय परिवार अक्सर ऋण और आर्थिक बोझ तले दबकर भी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए दहेज चुकाते हैं।
* निम्नवर्गीय समाज में भले ही रकम कम हो, परंतु वहाँ भी दहेज वस्त्र, आभूषण और घरेलू सामान के रूप में अनिवार्य समझा जाता है।
सामाजिक मूल्यांकन की आवश्यकता
दहेज की समस्या केवल आर्थिक लेन-देन की नहीं, बल्कि मानसिकता की है। यह मानसिकता हमें यह सोचने पर विवश करती है कि एक बेटा “बिकाऊ” है और बेटी का विवाह केवल “खरीद” के आधार पर संभव है।
निष्कर्ष
दहेज केवल विवाह की रस्म नहीं, बल्कि समाज के चरित्र का दर्पण है। जब तक बिरादरी और जातीय संगठनों में किसी आई.ए.एस. अधिकारी का अभिनंदन धनराशि के आधार पर होगा, और समाजसेवियों या डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा का मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक यह प्रथा खत्म नहीं हो पाएगी।
आवश्यक है कि हम सामूहिक रूप से इस प्रश्न पर विचार करें—
“क्या विवाह रिश्तों का बंधन रहेगा या सौदेबाज़ी का मंच?”
आइडिया 💡
श्री विजेंद्र कसाना जी
पाठ्य उन्नयन और विस्तार

प्रस्तुति