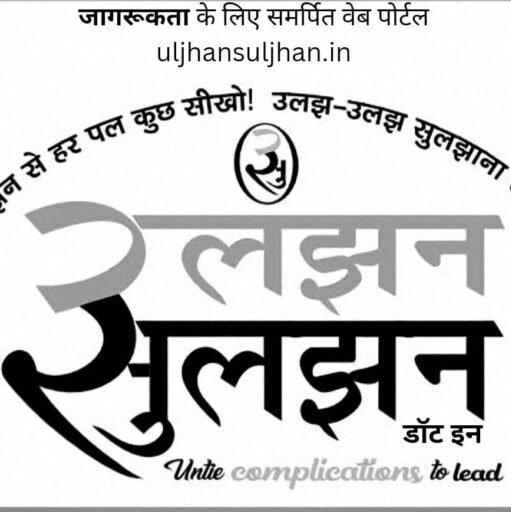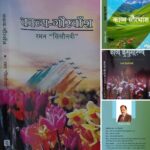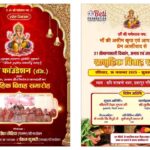तनाव – आधुनिक जीवन का मौन संकट

प्रोफेसर (डॉ.) विनोद शानवाल
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर तीसरा व्यक्ति तनावग्रस्त है। तनाव की जद में छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक सभी शामिल हैं। लंबे समय तक तनाव बने रहने से शरीर में गंभीर बीमारियाँ पनप सकती हैं। इसलिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए तनाव से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक तनाव न केवल सेहत के लिए बल्कि स्वयं जीवन के लिए भी खतरा है।
जब हम जीवन के हर पहलू को नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, हर बात को दबाव मानने लगते हैं और लगातार तनाव में रहने लगते हैं, तो समस्या गंभीर हो जाती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी कमजोर हो जाता है। वह न जीवन का आनंद ले पाता है, न ठीक से कार्य कर पाता है और न ही कुछ नया सोच पाता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति की जीने की इच्छा तक समाप्त होने लगती है। कई बार लोग आत्महत्या तक के बारे में सोचने लगते हैं।
निरंतर तनाव हार्ट अटैक, कैंसर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, माइग्रेन, सिरदर्द, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन जाता है। यह अनहेल्दी लाइफस्टाइल को भी बढ़ावा देता है, जैसे स्मोकिंग, शराब सेवन और अस्वस्थ आहार—जो शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुँचाते हैं।
तनाव की जड़ें कहाँ हैं, यह पहचानना बेहद आवश्यक है। इसकी जड़ें आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा में छिपी हैं। तनाव आधुनिक जीवन का मौन संकट है, जिसका समाधान सभी की प्राथमिकता होना चाहिए। तभी इक्कीसवीं सदी की इस मानसिक महामारी से निजात पाई जा सकती है।
आज का मनुष्य विकास की ऐसी दौड़ में शामिल हो चुका है जहाँ ठहराव का नाम लेना मानो अपराध है। बाज़ार, तकनीक, मीडिया और भौतिक साधनों की अट्टहास ने जीवन को अपने दबावों से जकड़ लिया है। देखने में सब कुछ सुविधाजनक प्रतीत होता है, पर यही सुविधाएँ बढ़ती दुविधाओं की जड़ बन चुकी हैं। इन्हीं के भीतर असुविधा का असली कारण छिपा है।
तनाव का सबसे बड़ा शिकार हमारे युवा बन रहे हैं, जिन्हें जीवन-संघर्षों से हरदम दो-चार होना पड़ता है। युवाओं की जीवनशैली जिस दिशा में ढल रही है, वह सचेत करने वाली है। जीवन में गति होना अच्छी बात है, पर जिस त्वरा को टेक्नोलॉजी और बाज़ारवाद ने जीवन को दी है, उससे जीवन का संतुलन डगमगा गया है। व्यक्ति मशीन की तरह जीने को अभिशप्त हो गया है। उसके पास अपने संबंधों, भावनाओं और आत्मसंवाद के लिए न समय है, न धैर्य।
तनाव आज केवल मानसिक दबाव नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम में प्रवेश कर चुका एक साइलेंट किलर है। तनाव की चपेट में केवल व्यक्ति नहीं, पूरा समाज है। परिवारों में संवादहीनता तलाक और पीढ़ीगत मतभेदों का कारण बन रही है। पढ़ाई का दबाव बच्चों को आत्महत्या जैसी चरम स्थितियों की ओर धकेल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाएँ युवाओं को तुलनात्मक सोच में सीमित कर रही हैं, वहीं सामाजिक तुलना की आग युवा मन को कुंठित कर रही है।
कार्यस्थल पर तनाव से उत्पादकता घट रही है, टीम भावना कमजोर हो रही है और असंतोष बढ़ रहा है। समाज में संवेदनाओं की कमी, हिंसा और अपराध प्रवृत्तियों में वृद्धि भी अप्रत्यक्ष रूप से तनाव की ही उपज है।
तनाव का एक प्रमुख कारण अव्यवस्थित जीवनशैली भी है। जब हम अपने समय का सही नियोजन नहीं करते, तो कार्यभार का दबाव जीवन की लय को तोड़ देता है। इसलिए आवश्यक है कि जीवन के हर चरण की प्राथमिकताएँ तय करें।
आत्मसंवाद और ध्यान करें। जब मन बिखरने लगे, तो उसे भीतर मोड़ें। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं से संवाद के लिए निकालें। योग, प्राणायाम और ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक सफाई की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।
सकारात्मक सोच और स्थितियों की स्वीकृति का अभ्यास करें, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। धैर्य और सजगता से परिस्थिति का सामना करें। अपना दृष्टिकोण अधिकतम सकारात्मक रखें।
तनाव के समाधान की राह जीवन के संतुलन से ही निकलेगी। तनाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन का हर मोड़ चुनौतीपूर्ण है, पर इसे संतुलन, स्वीकृति और सकारात्मकता से साधा जा सकता है।
समय प्रबंधन, जीवन की प्राथमिकताएँ तय करना, आपसी सहयोग और संबंधों को मजबूत रखना — यही संतुलन बनाए रखने के उपाय हैं। हमारा तनाव तब बढ़ता है जब हम अपने दुखों में अकेले पड़ जाते हैं। संवाद हर संकट की औषधि है। अपने परिजनों, मित्रों और सहकर्मियों से खुलकर बातें करें — इससे मन का बोझ हल्का होता है। एक सच्चा श्रोता हमें अवसाद से उबार सकता है।
तनाव से राहत के लिए श्वास-व्यायाम का नियमित अभ्यास करें, ध्यान करें, विश्राम करें, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। अपने किसी प्रिय से बात करें, कृतज्ञता का भाव बनाए रखें, और अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाएँ।
तनाव से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ — नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकालें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और विश्राम के लिए समय निकालना न भूलें।
निष्कर्षतः, तनाव से बचने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झाँकने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर की दौड़ को रोकना सीख लेंगे, तभी बाहरी होड़ से बच पाएँगे। सुख किसी सुविधा में नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और शांत मन में निहित है।
आधुनिक जीवन की इस उथल-पुथल में यदि मनुष्य यह समझ जाए कि —
“जीत से अधिक मूल्यवान है सफलता, और सफलता से भी अधिक आवश्यक है स्थिरता”
तो तनाव के तिरोहन के लिए हम तैयार रहेंगे, और तनाव स्वतः ही पराजित होता चला जाएगा।
🌱 एक शासकीय पहल है मनोदर्पण
मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सशक्त कदम
तनाव की इस महामारी के गंभीर संकट को समझते हुए भारत सरकार ने “मनोदर्पण” जैसी महत्वपूर्ण मुहिम की शुरुआत की है, जो मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है।
भारत सरकार द्वारा समर्थित यह एक-छत्र महान पहल छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। “मनोदर्पण” एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसे 27 जुलाई 2020 को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किया गया।
यह केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता तक सीमित नहीं, बल्कि मनो-सामाजिक सहायता तंत्र के विकास में भी सहायक है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को सशक्त बनाता है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (8448440632) की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई है।
साथ ही, सेमिनार, वेबिनार, समूह चर्चाओं और इंटरैक्टिव सत्रों की श्रृंखला निरंतर संचालित है, जिनका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी चिंताओं से निपटने के तरीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
यह मंच मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के सहयोग से मनो-सामाजिक सहायता प्रदान कर रहा है।
छात्रों के मार्गदर्शन हेतु पीएम ई-विद्या चैनल पर प्रतिदिन शाम 5 से 5:30 बजे तक ‘ सहयोग ‘ नामक लाइव इंटरैक्टिव सत्र प्रसारित होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को तनाव, चिंता, अवसाद और भावनात्मक समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करना है।
तनाव
आधुनिक जीवन का मौन संकट और उसका समाधान
(समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषणात्मक आलेख)

डॉ. राकेश राणा
आज का मनुष्य विकास की उस दौड़ में सम्मिलित है, जहाँ ठहराव का नाम लेना मानो अपराध है। विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की प्रचुरता ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसी सुविधा के भीतर छिपा है असुविधा का सबसे बड़ा कारण — तनाव। आधुनिक मनुष्य के पास सब कुछ है, सिवाय मानसिक शांति के। वह चल रहा है, दौड़ रहा है, जीत भी रहा है, परंतु भीतर से हारता जा रहा है।
तनाव की जड़ें
आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा में खोया मनुष्य
बीते दशकों में मानव सभ्यता ने जिस तीव्रता से गति पकड़ी है, उसने जीवन की दिशा को ही बदल दिया है। “समय ही धन है” की अवधारणा ने मनुष्य को इतनी तेजी से काम करने पर विवश कर दिया कि वह खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा। हर व्यक्ति एक मशीन की तरह जीवन जी रहा है, जिसके पास भावनाओं, संबंधों और आत्मसंवाद के लिए न समय है, न धैर्य।
उदाहरण के लिए, महानगरों में सुबह से रात तक ऑफिस की भागदौड़ में लगे लोग सप्ताहांत का इंतजार इसीलिए करते हैं कि दो दिन “थोड़ा चैन” मिल सके। लेकिन यह चैन भी मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया की डिजिटल बेड़ियों में जकड़ा रहता है।
तनाव के प्रकार और स्वरूप
तनाव केवल मानसिक दबाव नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम में प्रवेश कर चुका एक मौन रोग है।
1. व्यक्तिगत तनाव — व्यक्ति की असफलताएं, अपेक्षाएं और अधूरी इच्छाएं उसे भीतर से तोड़ती हैं।
2. पारिवारिक तनाव — संयुक्त परिवारों के विघटन और संवाद की कमी ने रिश्तों में दूरी बढ़ाई है।
3. सामाजिक तनाव — समाज में दिखावे, प्रतिष्ठा और तुलना की भावना ने आत्ममूल्यांकन को विकृत किया है।
4. व्यावसायिक तनाव — नौकरी की अनिश्चितता, लक्ष्य का दबाव और समय की कमी ने कार्यस्थलों को तनाव का केंद्र बना दिया है।
भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज़ (NIMHANS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, हर चार में से एक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर तनावग्रस्त है। और यह आंकड़ा केवल शहरी भारत का नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी अब इस चपेट में आ चुके हैं।
भौतिक उन्नति बनाम मानसिक पतन
यह एक विडंबना है कि जितनी तेज़ी से हमने भौतिक स्तर पर प्रगति की है, उतनी ही तीव्रता से मानसिक शांति खोई है।
पहले लोग कम संसाधनों में भी सुखी थे, क्योंकि उनमें आभार, संतोष और सह-अस्तित्व की भावना थी। आज जब सब कुछ उपलब्ध है, तब भी “संतोष” अनुपस्थित है।
मनुष्य ने अपने लिए आलीशान घर बनाए, पर मन की शांति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा।
यह वही स्थिति है, जिसे कवि अज्ञेय ने कहा था —
“हम बढ़े साधन, घटा साध्य। बढ़ी वाणी, घटा संवाद।”
तनाव के सामाजिक प्रभाव
तनाव केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करता है।
परिवार में संवादहीनता, तलाक की बढ़ती दरें और पीढ़ीगत मतभेद इसी का परिणाम हैं।
शिक्षा में विद्यार्थियों का आत्महत्या की ओर झुकाव, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और सामाजिक तुलना की आग युवाओं की मानसिकता को कुंठित कर रही है।
कार्यस्थल पर तनाव से उत्पादकता घट रही है, टीम भावना कमजोर पड़ रही है और असंतोष बढ़ रहा है।
समाज में संवेदनाओं की कमी, हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति में वृद्धि भी अप्रत्यक्ष रूप से तनाव की ही उपज है।
तनाव के समाधान की राह
जीवन में संतुलन की खोज
तनाव को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन का हर मोड़ चुनौतीपूर्ण है। परंतु इसे संतुलन, स्वीकृति और सकारात्मकता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
1. समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण
तनाव का एक बड़ा कारण है — अव्यवस्थित जीवनशैली।
जब व्यक्ति अपने समय को सही दिशा में नियोजित नहीं करता, तो कार्यभार का दबाव उसे तोड़ देता है।
इसलिए आवश्यक है कि हम ज़रूरी कार्य पहले, और अनावश्यक कार्य बाद में की नीति अपनाएँ।
2. आत्मसंवाद और ध्यान
जब मन बिखरने लगे, तो उसे भीतर मोड़िए। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं से संवाद में बिताइए।
योग, प्राणायाम और ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मस्तिष्क की सफाई की प्रक्रिया हैं।
आईआईटी खड़गपुर की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, नियमित ध्यान करने वाले व्यक्तियों में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर 35% तक कम पाया गया।
3. सकारात्मक सोच और स्वीकृति का अभ्यास
जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है।
यदि हम असफलता को भी सीखने का अवसर मान लें, तो तनाव का असर बहुत घट जाता है।
स्वामी विवेकानंद का यह कथन याद रखना चाहिए —
“जीवन में हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है, न कि तोड़ने।”
4. सामाजिक जुड़ाव और संवाद
तनाव तब बढ़ता है जब व्यक्ति अपने दुखों में अकेला पड़ जाता है।
संवाद सबसे बड़ी औषधि है। परिवार, मित्रों और सहकर्मियों से खुलकर बात करना मानसिक बोझ को कम करता है।
कई बार केवल एक सच्चे श्रोता की उपस्थिति व्यक्ति को अवसाद से उबार सकती है।
5. प्रकृति से जुड़ाव
प्रकृति सर्वोत्तम चिकित्सक है। पेड़-पौधों के बीच कुछ समय बिताना, सूर्योदय देखना या वर्षा में भीगना — यह सब मस्तिष्क को नई ऊर्जा देता है।
जापान में इसे “Forest Bathing” कहा जाता है, जहाँ लोग जंगल में सैर कर तनाव घटाते हैं।
6. संतोष और कृतज्ञता का भाव
कृतज्ञता का अभ्यास मनुष्य को भीतर से स्थिर करता है।
हर रात सोने से पहले तीन बातों के लिए “धन्यवाद” कहना — यह छोटी-सी आदत तनाव के विरुद्ध एक बड़ी दीवार बन जाती है।
उदाहरण : एक प्रेरक दृष्टांत
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन तनाव प्रबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है।
कठिन परिस्थितियों, वैज्ञानिक जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय अपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की।
उनका कहना था —
“यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखिए।”
उन्होंने तपस्या को स्वीकार किया, प्रतिकूलताओं को अवसर में बदला — यही वास्तविक तनाव-मुक्त जीवन की पहचान है।
निष्कर्ष
तनाव से बचने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झाँकने की आवश्यकता है।
जब हम अपने भीतर की दौड़ को रोकना सीख जाएँगे, तभी बाहरी भागदौड़ का असर कम होगा।
वास्तविक सुख किसी विलास में नहीं, बल्कि संतुलित और शांत मन में है।
आधुनिक जीवन की इस उथल-पुथल में यदि मनुष्य यह समझ ले कि “सफलता से अधिक आवश्यक है स्थिरता”, तो तनाव स्वतः ही पराजित हो जाएगा।
“मनुष्य ने अंतरिक्ष को जीत लिया,
पर अपने ही मन की शांति हार बैठा।
अब समय है कि वह भीतर लौटे,
क्योंकि वहीं छिपा है — वास्तविक सुख का स्रोत।”
यह आलेख समाज को यह सिखाता है कि तनाव का समाधान तकनीक में नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि में है।
जब तक मनुष्य संतुलन, करुणा और आत्मसंवाद का मार्ग नहीं अपनाएगा, तब तक भागदौड़ भरी जिंदगी का यह तनाव उसका मौन शत्रु बना रहेगा।
(लेखक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध एम.एम.एच. कॉलेज में समाजशास्त्र विषय के शिक्षक हैं।)
सूचना स्रोत
डॉ राकेश राणा
पाठ्य उन्नयन, संशोधन और प्रस्तुति